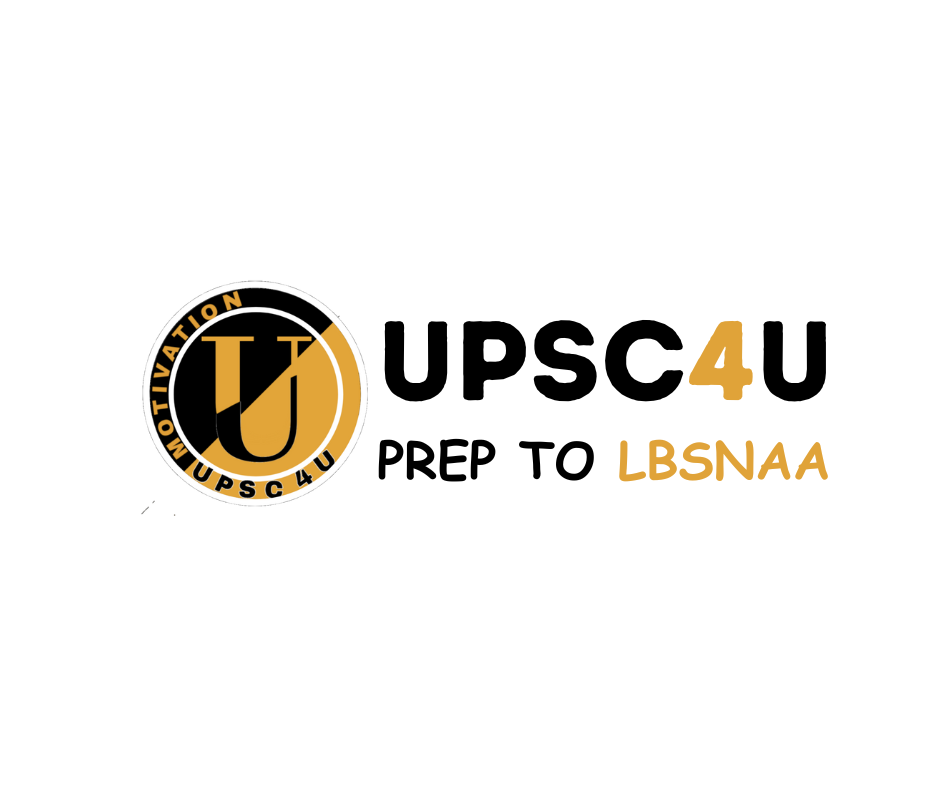भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित है।
- भितरकनिका ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी नदी प्रणालियों के मुहाने में स्थित एक समृद्ध व जीवंत इको-प्रणाली है।
- इसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यह रामसर स्थल है।
- इसे वर्ष 1988 में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था।
- यहाँ सफेद मगरमच्छ काफी अधिक संख्या में पाये जाते हैं। इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को सफेद मगरमच्छ पार्क भी कहा जाता है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है।
- यह ओडिशा के बेहतरीन जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है और अपने मैंग्रोव, प्रवासी पक्षियों, कछुओं, मुहाना के मगरमच्छों तथा अनगिनत खाड़ियों के लिये प्रसिद्ध है।
- ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देश के मुहाना या खारे जल के मगरमच्छों का 70% हिस्सा रहता है, जिसका संरक्षण वर्ष 1975 में शुरू किया गया था।
संरक्षित क्षेत्र
सफेद या एश्चुअरी मगरमच्छ
- भारत में मगरमच्छ की तीन प्रजातियां पाई जाती हैं- मगर या दलदली(मार्श) मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ(एश्चुअरी मगरमच्छ ) और घड़ियाल।
- एश्चुअरी मगरमच्छ को ही सफ़ेद मगरमच्छ भी कहा जाता है।
- एश्चुअरी मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ हैं। भारत में ये सबसे अधिक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाये जाते हैं।
- भितरकनिका के अलावा, एश्चुअरी मगरमच्छ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी बहुतायत में पाये जाते हैं।
- एश्चुअरी मगरमच्छ को आईयूसीएन की ‘कम चिंतनीय’ सूची में शामिल किया गया है।
- गौरतलब है कि घड़ियाल व एश्चुअरी मगरमच्छ दोनों के संरक्षण कार्यक्रम को पहली बार 1975 में ओडिशा में ही लागू किया गया था।
क्या होते हैं प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ
प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ
- कोरल रीफ़ को प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है।
- ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्सियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं।
- कोरल रीफ़ प्रायः उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं, जहाँ तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस रहता है।
- ये शैल-भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच छिछले लैगून बन जाते हैं।
- कोरल या प्रवाल उथले सागर में पाए जाते हैं और इनके विकास के लिये स्वच्छ एवं अवसादरहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं।
- प्रवाल या कोरल्स फोटोसिंथेटिक शैवाल के साथ पारस्परिक रूप से साथ में रहते हैं, जिसे जूजैन्थेला कहा जाता है।
- कोरल(मूंगा) प्रवाल भित्तियों के लिए एक मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट संरचना बनाते हैं और जूजैन्थेला के लिए सुरक्षा और एक घर प्रदान करते हैं। इसके बदले मे जूजैन्थेला मूंगा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
- जब महासागर की सतह एक सीमा से अधिक गरम हो जाती है, तब कोरल जूजैन्थेला को बाहर निकाल देता है, जिससे ‘प्रवाल विरंजन’ या कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है।
- कोरल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बढती मात्रा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान का बढ़ना, महासागरों का अम्लीकरण, मछलियों का अधिक शिकार होने के कारण काफी नुकसान होता है।
प्रवाल भित्ति के प्रकार
- कोरल रीफ़ मूलतः तीन प्रकार की होती हैं:
- तटीय या झालरदार कोरल रीफ़
- अवरोधक कोरल रीफ़
- एटॉल।
तटीय कोरल रीफ़
- महाद्वीपीय या द्वीपीय तट से लगी कोरल रीफ़ को तटीय कोरल रीफ़ कहा जाता है।
- समान्यतः ये भित्तियाँ तट से सटी रहती हैं परन्तु कभी-कभी इनके एवं स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटे लैगून का निर्माण हो जाता है, जिसे बोट चैनल कहा जाता है।
- चट्टानों के टुकड़ों, मृत प्रवालों और मिट्टी से निर्मित होती हैं, जीवित प्रवाल इनके बाहरी किनारों एवं ढलानों पर पाए जाते हैं।
- भारत में ये मन्नार की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं।
अवरोधक कोरल रीफ़
- इस प्रकार की कोरल रीफ़ तटों से कुछ दूरी पर होती हैं, इनका विकास तट के समानांतर होता है।
- ये समुद्र और स्थल भाग के बीच लंबी अवरोधक दीवारों का निर्माण करते हैं। स्थल और कोरल रीफ़ के बीच सैकड़ों मीटर चौड़े लैगून बने होते हैं।
- संसार की सबसे बड़ी अवरोधक कोरल रीफ़ ऑस्ट्रेलिया की ‘ग्रेट बैरियर रीफ’ है।
एटॉल
- इन्हें वलयकार कोरल रीफ़ या एटॉल भी कहा जाता है।
- ये किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होता है।
- ये अँगूठी या घोड़े के नाल की आकृति वाली होती हैं। इनके केन्द्र में लैगून होता है। इनके बीच-बीच में खुले भाग पाए जाते हैं जिस कारण खुले सागर और लैगून का संपर्क बना रहता है।
- वलयाकार प्रवाल भित्ति के प्रमुख उदाहरण हैं-फिजी एटॉल, भारत का लक्षद्वीप समूह में भी अनेक एटॉल पाए जाते हैं।
वितरण
- दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रवाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ प्रवाल दक्षिणी फिलिपींस से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यू गिनी तक पाए जाते हैं।
- प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया, वानुआतु, पापुआ न्यू गिनी में भी प्रवाल पाए जाते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है।
- भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि द्वीप भी प्रवालों से बने हुए हैं। प्रवाल लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी पाए जाते हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});