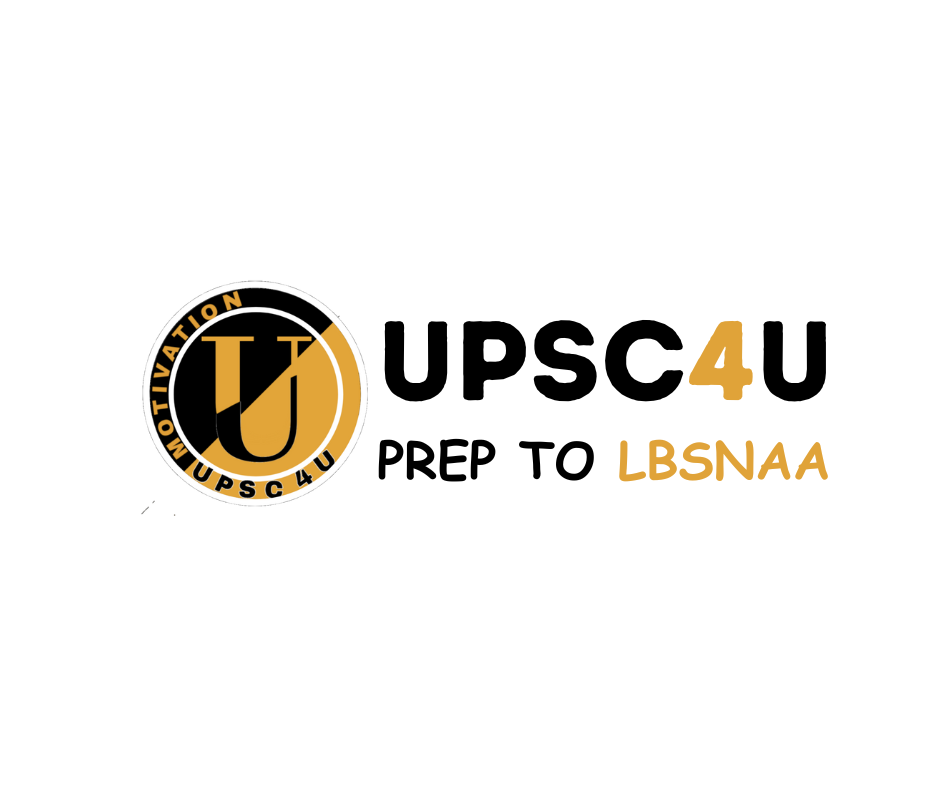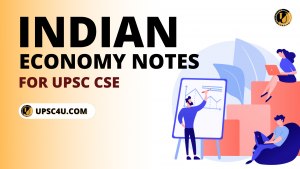कृषि साख
- कृषि साख से तात्पर्य है कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध वित्त| यह मुख्यता दो स्त्रोतों से प्राप्त होता है -प्रथम संस्थागत स्रोत और दूसरा गैर संस्थागत स्त्रोत |
- सरकार वाणिज्य बैंक को तथा सहकारी बैंक का आदि संस्थागत स्त्रोत के उदाहरण हैं जबकि गैर संस्थागत स्त्रोत के अंतर्गत ग्रामीण साहूकार, महाजन इत्यादि को शामिल किया जाता है |
- किसानों द्वारा सामान्यता तीन प्रकार का ऋण लिया जाता है |
- अल्पकालीन ऋण, जो कि 15 महीने से कम अवधि के लिए होता है |
- मध्यकालीन ऋण, जो कि 15 महीने से 5 वर्ष के लिए होता है |
- दीर्घकालीन ऋण, जो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होता है |
- किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण बीज, खाद, पशुचारा आदि के लिए लिया जाता है |
- जबकि मध्यकालीन ऋण पशु खरीदने छोटे औजार खरीदने के लिए लिया जाता है |
- खेत महंगी मशीन आदि खरीदने के लिए किसानों द्वारा दीर्घकालीन ऋण लिया जाता है
भूमि विकास बैंक
- किसानों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई |
- यह बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थाई सुधार करने अथवा ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है |
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई यह बैंक की कृषि के लिए साख उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण संस्था है |
- केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 के बाद से कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का योगदान बढ़कर 65% से अधिक हो चुका है |
- कृषि क्षेत्र को संस्थागत संस्थानों द्वारा दिए गए कुल ऋण में सर्वाधिक योगदान वाणिज्य बैंकों (74%) का है उसके बाद क्रमशः सहकारी बैंक को (17%) व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (9%) का स्थान आता है |
- केंद्रीय नीति के अनुसार निजी एवं सार्वजनिक बैंकों को अपने द्वारा दिए गए कोई निर्णय में से 40% प्राथमिक क्षेत्र को प्रदान करना अनिवार्य है |
- प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित कुल ऋण में से 18% कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान करना अनिवार्य किया गया है |
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
- वर्ष 1999-2000 में रवि फसल से इस योजना की शुरुआत की गई इसे व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर आरंभ शुरू किया गया |
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, आग लगना, कीटों की बीमारियों आदि के कारण फसल नष्ट होने से किसान को हुए नुकसान की भरपाई करना है खरीफ और रबी फसल के अंतर्गत कुल 70 फसलों को उसके दायरे में लाया गया है |
- यह योजना सभी किसानों के लिए है इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम भुगतान में 10% की सब्सिडी दी जाती है |
- जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है कुछ राज्य सरकारें किसानों को 10% से अधिक सब्सिडी भी दे रही हैं |
मौसम आधारित फसल बीमा योजना
- मौसम पर आधारित खरीफ को वर्ष 2007-08 प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा है इस योजना का उद्देश्य पैदावर पर विपरीत प्रभाव डालने वाली मौसमी घटनाओं से किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है |
- राज्य सरकारों द्वारा बुवाई के मौसम से पूर्व फसलों और संदर्भित इकाई क्षेत्र अधिसूचित किए जाते हैं |
- प्रत्येक इकाई क्षेत्र के संदर्भ मौसम केंद्र से संबंध होता है जिसके आधार पर दावे निपटाए जाते है |
- किसी मौसम केंद्र द्वारा मापित मौसम के उतार-चढ़ाव के आधार पर भुगतान किए जाते हैं दावे सत्र आधार पर स्वर निपटाए जाते हैं और किसानों को नुकसान की सूचना अथवा दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है |
विपणन प्रणाली क्या होती है ?
विपणन प्रणाली
- कृषि पदार्थों का संग्रहण भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि को वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है |
- भारत में कृषि उत्पादों के संबंध में विपणन व्यवस्था भारत में खाद्य पदार्थों का विपणन मुख्यतः नियमित बाजारों के माध्यम से होता है |
- यह बाजार राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार द्वारा बनाया जाता है, यहां कुछ वस्तु अथवा विशिष्ट वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है |
- इनके अलावा कृषि विपणन के लिए सहकारी विपणन समितियां भी महत्वपूर्ण है इसका निर्माण 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर अपने उत्पादों के विक्रय के लिए करते हैं |
राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ
- इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी यह एक शीर्ष सरकारी संगठन है, जो कुछ चुने गए कृषि उत्पादों की खरीद वितरण निर्यात तथा आयात में सलंग्न है |
- यह राज्यों के बीच कृषि उत्पादन के व्यापार को भी परिवर्तित करता है, यह अदरक, लहसुन, प्याज, दाल इत्यादि वस्तुओं का निर्यात तथा देश के किसी भाग में इन वस्तुओं की कमी की पूर्ति करता है |
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद
- इस परिषद की स्थापना 1987 में की गई थी इसका उद्देश्य जनजातियों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलवा कर उन्हें व्यापारियों के शोषण से बचाना है |
वेयर हाउसिंग
- उत्पादन के स्थान से बाजार तक ले जाने की क्रिया के दौरान वस्तुओं को रखने वाले गोदाम को वेअरहाउसिंग कहा जाता है| कृषि उत्पादों के भंडार और वेअरहाउसिंग से जुड़ी हुई वर्तमान में 3 संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं