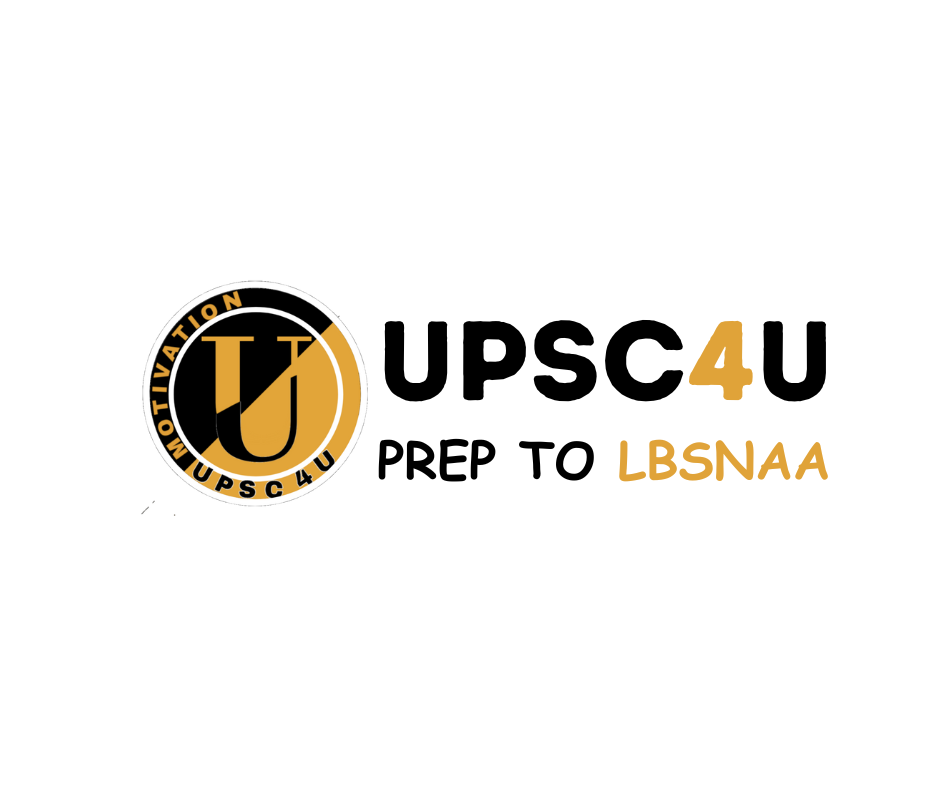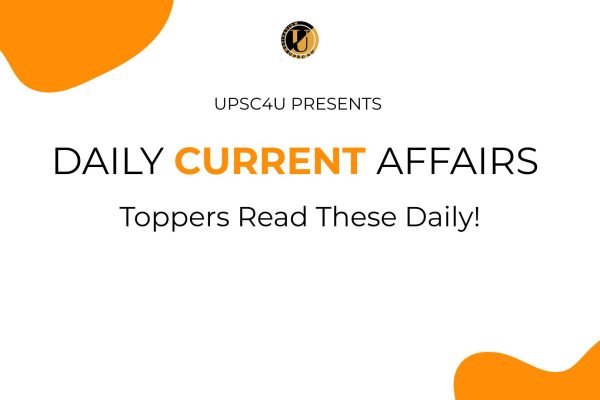समुद्री क्षेत्र में नए खतरे और चुनौतियाँ, जिनमें अपरंपरागत सुरक्षा खतरे, अवैध मछली पकड़ना, प्राकृतिक आपदाएँ, समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शामिल हैं।
हाल के वर्षों में समुद्री क्षेत्र में कठिन सुरक्षा चुनौतियों ने एक नया आयाम ले लिया है।
अवैध मछली पकड़ना, प्राकृतिक आपदाएँ, समुद्री प्रदूषण, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी और जलवायु परिवर्तन जैसे अपरंपरागत सुरक्षा खतरे समुद्री क्षेत्र में मुख्य चिंताएँ हैं।

केवल सैन्य साधनों का उपयोग करके इन खतरों से प्रभावी ढंग से नहीं लड़ा जा सकता है।
राज्यों को इन सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक पूंजी, संसाधन और विशेषज्ञ कर्मियों को प्रतिबद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
भारत अपने जी20 की अध्यक्षता के दौरान समुद्री सुरक्षा पर चर्चा में ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर जोर देता रहा है।
समुद्र में गैर-पारंपरिक खतरों से लड़ने के लिए फिलहाल कोई कामकाजी खाका नहीं है।
तटीय क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्य अवास्तविक बने हुए हैं क्योंकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के तटीय राज्यों की आवाज को विकसित देशों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
वैश्विक दक्षिण में तटीय राज्यों को अंतर-क्षेत्राधिकार संबंधों और परस्पर सुरक्षा लक्ष्यों के कारण समुद्री शासन के उद्देश्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
समुद्र के बढ़ते स्तर, समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ वैश्विक दक्षिण में कम विकसित राज्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे वे असुरक्षित हो जाते हैं।
एशिया और अफ्रीका के तटीय राज्यों में समुद्री खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा समन्वय और असमान कानून-प्रवर्तन क्षमताओं का अभाव है।
कुछ राज्य विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए भागीदार देशों के साथ समुद्री सहयोग का विरोध करते हैं।
तटीय राज्य सामान्य न्यूनतम सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भागीदार देशों के साथ जानकारी साझा करने के इच्छुक हैं।
भारत का समुद्री विज़न 2030 विकास और आजीविका उत्पन्न करने के लिए बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने पर केंद्रित है।
इंडो-पैसिफिक पर ढाका का उद्घाटन आधिकारिक दस्तावेज़ समुद्री सुरक्षा के लिए एक विकासात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
अफ्रीका एक संपन्न नीली अर्थव्यवस्था और एक सुरक्षित समुद्री क्षेत्र के महत्व पर भी चर्चा कर रहा है।
एशिया और अफ्रीका में अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसमें अवैध रूप से दर्ज न की गई और अनियमित मछली पकड़ने की संख्या में वृद्धि हुई है।
दोषपूर्ण नीतियां, उदार नियम, ढीला कानून प्रवर्तन और हानिकारक सब्सिडी अवैध मछली पकड़ने की समस्या में योगदान करती हैं।
भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण, आपदा जोखिम में कमी और समुद्री कनेक्टिविटी सहित समुद्री चुनौतियों का समाधान प्रस्तावित करती है।
इस पहल को प्रमुख इंडो-पैसिफिक राज्यों और कई पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है।
समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक रणनीति लागू करना चुनौतीपूर्ण है
समुद्री एजेंसियों को अंतरसंचालनीयता में सुधार करने, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षेत्रीय नियम-आधारित आदेश पर सहमत होने की आवश्यकता है
राज्यों को समुद्री सुरक्षा संचालन के एकीकृत स्वरूप को अपनाना होगा और घरेलू विनियमन को अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ जोड़ना होगा
वैश्विक दक्षिण में कई तटीय राज्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के ठोस समाधान के लिए अनिच्छुक हैं
विकासशील देशों को समुद्र में सामूहिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे सामूहिक कार्रवाई पर राजनीतिक और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देते हैं।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) बनाने का प्रस्ताव और न्यायपालिका की विविधता और दक्षता पर इसका संभावित प्रभाव। यह जिला न्यायाधीशों की भर्ती की वर्तमान प्रणाली और कानूनी शिक्षा में केंद्रीकरण और एकरूपता से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डालता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका में विविधता लाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के निर्माण का सुझाव दिया।
एआईजेएस विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीश बनने की अनुमति देगा।
एआईजेएस के विचार पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और यह वर्षों से केंद्र सरकार में आधिकारिक नीति पर चर्चा का हिस्सा रहा है।
प्रस्ताव पर कोई आम सहमति नहीं है, केवल दो उच्च न्यायालय इस पर सहमत हैं और 13 इसके विरुद्ध हैं।
उच्च न्यायालयों के माध्यम से जिला न्यायाधीशों और लोक सेवा आयोगों के माध्यम से अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की वर्तमान प्रणाली विविधता सुनिश्चित करने के लिए अधिक अनुकूल है।
वर्तमान प्रणाली आरक्षण और स्थानीय प्रथाओं और स्थितियों की स्पष्ट समझ दोनों की अनुमति देती है।
न्यायाधीशों को न्यायिक कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ होना आवश्यक है, सिविल सेवा के विपरीत जहां उन्हें अनुभवी निचली नौकरशाही द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के निर्माण की अनुमति देता है।
एआईजेएस के निर्माण के लिए राज्यों की परिषद से दो-तिहाई बहुमत वाला एक प्रस्ताव और एक संसदीय कानून की आवश्यकता होती है
प्रस्ताव में राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाले नियमों को खत्म करने के लिए एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता होगी
यह संभावना नहीं है कि सभी राज्य अपने क्षेत्र से किसी अन्य विषय के केंद्रीकरण के लिए सहमत होंगे
एआईजेएस 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के साथ, जिला न्यायाधीशों के पद से कमतर न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय सेवा की पेशकश करेगा।
हालाँकि, कानूनी शिक्षा में देशव्यापी एकरूपता की कमी और अकादमिक प्रतिभा पर व्यावहारिक अनुभव को प्राथमिकता युवा वकीलों को एआईजेएस के लिए आवेदन करने से रोक सकती है।
शीर्ष लॉ स्कूल स्नातकों के राष्ट्रीय न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में बैठने की संभावना नहीं है, क्योंकि मुकदमेबाजी, कानून फर्मों में शामिल होना और कॉर्पोरेट क्षेत्र जैसे विकल्प अधिक फायदेमंद लग सकते हैं।
कैरियर की प्रगति पर निश्चितता की कमी, क्योंकि उच्च न्यायालयों में पदोन्नत जिला न्यायाधीशों की संख्या बार के न्यायाधीशों की तुलना में कम है, एआईजेएस को अनाकर्षक भी बना सकती है।
पार्टियों के आगामी सम्मेलन (सीओपी) और जलवायु परिवर्तन पर देशों द्वारा कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता। यह वैश्विक उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति और पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं करने के परिणामों पर प्रकाश डालता है।

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) का 28वां संस्करण अगले पखवाड़े में हो रहा है।
सम्मेलन का लक्ष्य 190 देशों को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित करना है।
2015 में पेरिस में की गई सामूहिक प्रतिबद्धता सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रखने की थी।
इस प्रतिबद्धता के बावजूद, 2021-22 से उत्सर्जन वास्तव में 1.2% बढ़ गया है।
यदि उत्सर्जन इसी दर से जारी रहा तो सदी के अंत तक दुनिया 2.5-3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगी।
इस वर्ष वैश्विक तापमान के 1.5°C की सीमा पार करने के 86 मामले पहले ही सामने आ चुके हैं।
सीओपी बैठकों में प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं तीन सिद्धांतों पर सहमत हुई हैं: तेजी से औद्योगिकीकृत देशों द्वारा असंगत कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण की आवश्यकता, और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने वाले विकासशील देशों के लिए मुआवजा।
आपसी संदेह, डी-वैश्वीकरण और राजनीतिक प्रतिशोध के डर के कारण सभी देशों को इन सिद्धांतों पर कार्य करने में चुनौती निहित है।
COP28 में जिन दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, वे हैं ग्लोबल स्टॉकटेक का निष्कर्ष और हानि और क्षति कोष का संचालन।
फंड के आकार और देशों द्वारा व्यक्तिगत योगदान पर कोई स्पष्टता नहीं है।
COP28 को केवल चेतावनियों के साथ समझौते देने के बजाय हस्ताक्षरकर्ताओं को निश्चित कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करना चाहिए।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का आगामी सम्मेलन (COP28)। यह उन प्रमुख मुद्दों की पड़ताल करता है जिन्हें सम्मेलन में संबोधित किया जाएगा, जैसे ग्लोबल स्टॉकटेक, जीवाश्म ईंधन का प्रश्न, अनुकूलन और वित्त।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 28वां वार्षिक सम्मेलन (COP28) दिसंबर की शुरुआत में दुबई में होगा।
सीओपी वह केंद्रीय स्थान है जहां वैश्विक जलवायु प्रशासन पर चर्चा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं।

सभी देशों, न कि केवल शक्तिशाली देशों की, सीओपी में अपनी बात होती है, जो समानता और भेद्यता पर चर्चा की अनुमति देती है।
2023 में अत्यधिक गर्मी, जंगल की आग, बाढ़ और सूखा जैसी विनाशकारी मौसमी घटनाएं देखी गई हैं, जिससे यह रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत दृष्टिकोण और इसके लिए भुगतान कौन करेगा, इस पर असहमति अनसुलझी बनी हुई है।
अमेरिका और चीन के बीच तनाव और यूक्रेन और गाजा में संघर्ष के साथ, भू-राजनीतिक संदर्भ सहयोग बढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है।
सीओपी में राजनयिकों को वैश्विक सहयोग के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक जरूरी समस्या का समाधान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
सीओपी में अक्सर बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती।
लेख में दुबई के सीओपी की अपेक्षाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।
ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) पेरिस समझौते की मशीनरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जीएसटी जलवायु कार्रवाई के लिए शमन, अनुकूलन और समर्थन में समग्र प्रगति का आकलन करता है।
जीएसटी का मानना है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मार्ग पेरिस लक्ष्यों तक वार्मिंग को सीमित करने के रास्ते पर नहीं हैं।
विकासशील देशों का तर्क है कि जीएसटी को विकसित देशों को जलवायु कार्रवाई में उनकी पिछली विफलताओं के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए।
विकसित देशों का तर्क है कि भविष्य में होने वाले उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा विकासशील देशों पर पड़ेगा और जीएसटी को आगे चलकर उत्सर्जन को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इस बहस के नतीजे कार्रवाई के लिए भविष्य के मानदंड निर्धारित करेंगे, जिसमें विकसित देशों के लिए विकासशील देशों की तुलना में पहले शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की उम्मीद भी शामिल है।
जीएसटी का लक्ष्य 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नामक निचले स्तर की राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं के अगले दौर को सूचित करना और संचालित करना है।
इस बात पर बहस चल रही है कि क्या जीएसटी को अनुदेशात्मक होना चाहिए और इसके लिए विशिष्ट प्रकार की प्रतिज्ञाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि पूर्ण उत्सर्जन लक्ष्य और विशिष्ट तापमान लक्ष्यों के साथ संरेखण।
कुछ लोगों का तर्क है कि प्रगति में तेजी लाने के लिए नुस्खे की आवश्यकता है, लेकिन अन्य लोग इसके खिलाफ तर्क देते हुए कहते हैं कि इसमें इस बात पर सहमति नहीं है कि प्रत्येक देश को उत्सर्जन को सीमित करने के लिए क्या करने के लिए कहा जा सकता है।
जीएसटी में प्रतिज्ञाओं के संवर्धित कार्यान्वयन का भी आह्वान किया गया है, भविष्य के इरादे के बयानों के बजाय उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जो देश अभी कर सकते हैं।
सीओपी में देशों से नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने का आह्वान करने वाली भाषा शामिल होने की संभावना है, जैसा कि हाल ही में जी20 दिल्ली नेताओं की घोषणा में कहा गया है।
भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोयला ही नहीं, बल्कि सभी जीवाश्म ईंधनों पर व्यापक ध्यान देने की वकालत करता है।
विकसित दुनिया में तेल और गैस ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं और दुबई जैसे पेट्रोस्टेट के लिए महत्वपूर्ण हैं।
‘जीवाश्म ईंधन’ से पहले ‘अनएबेटेड’ शब्द जोड़ने से पौधों को उत्सर्जन को पकड़ने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे जीवाश्म ईंधन को लंबा जीवन मिल सकता है।
COP28 अनुकूलन और वित्त पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें ‘अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य’ पर सहमति होगी।
अनुकूलन प्रयासों के लिए ‘कौन भुगतान करता है’ का प्रश्न प्रमुख होने की संभावना है, पिछले सीओपी के बाद से अनुकूलन वित्त को दोगुना करने की मांग की जा रही है।
COP28 में हानि और क्षति कोष की स्थापना एक प्रमुख मुद्दा है।
इस बात पर कमजोर सहमति बन गई है कि फंड में कौन भुगतान करेगा (विकसित देश) और कौन प्राप्त करेगा (विशेष रूप से कमजोर देश)।
विश्व बैंक को फंड के अंतरिम मेजबान के रूप में सहमत किया गया है, लेकिन सख्त शासन दिशानिर्देशों के साथ।
कम ट्रिलियन की संख्या के साथ, चर्चा शमन और अनुकूलन का समर्थन करने की जरूरतों के ठोस मूल्यांकन पर केंद्रित हो गई है।
सार्वजनिक बनाम निजी फंड की भूमिका और वैश्विक वित्तीय माहौल में बड़े बदलाव की आवश्यकता सहित, धन कैसे जुटाया जाएगा, इसके बारे में विवादास्पद मुद्दे बने हुए हैं।
जलवायु परिवर्तन अब भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक उच्च पटल पर चर्चा का विषय है।
सीओपी में देशों के लिए दांव जलवायु प्रभावों, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा राजनीति और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में परिणामी हैं।
दुबई COP28 वैश्विक जलवायु राजनीति के धीमे विकास में एक महत्वपूर्ण मार्कर होगा।
भारत सहित विभिन्न देशों में बिजली उत्पादन में स्वच्छ और जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी। यह स्वच्छ ऊर्जा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में चीन और ब्राजील जैसे देशों द्वारा की गई प्रगति के साथ-साथ भारत और सऊदी अरब जैसे देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन यूएनएफसीसीसी की “साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों” की अवधारणा के माध्यम से अधिक जलवायु वित्तपोषण और इक्विटी की मांग कर रहे हैं।
चीन ने बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की अपनी हिस्सेदारी 2000 में 82% से घटाकर 2022 में 65% कर दी है, लेकिन यह अभी भी स्वच्छ और गंदी ऊर्जा दोनों में दुनिया में अग्रणी है।
स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है, बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 17% से बढ़कर 23% हो गई है।
ब्रिक्स देशों में सऊदी अरब में जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्पादित बिजली का प्रतिशत सबसे अधिक है, जिसमें 99% से अधिक जीवाश्म ईंधन से आता है, जिसमें से 67% गैस से होता है।
यूएई ने बिजली मिश्रण में परमाणु ईंधन को शामिल करने के साथ 2020 के बाद अपनी स्वच्छ ऊर्जा हिस्सेदारी में सुधार किया है।
ब्रिक्स में ब्राजील और इथियोपिया ही ऐसे दो देश हैं जहां बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी से अधिक है।
ब्राज़ील ने कार्बन क्रेडिट बाज़ारों के नियमों और अपने विशाल जंगलों के मुद्रीकरण की योजना पर बातचीत का नेतृत्व किया है।
दक्षिण अफ्रीका ने कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित होने के लिए 8.5 अरब डॉलर का सौदा हासिल किया है लेकिन वर्तमान में वह बिजली संकट का सामना कर रहा है।
गुजरात और राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में गिरावट दर्ज की गई है।
भारत के शीर्ष 15 बिजली उत्पादक राज्यों में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा में हिस्सेदारी अधिक है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार की बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 90% से अधिक रही है।
ओडिशा और पंजाब में हाल के वर्षों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि देखी गई है।