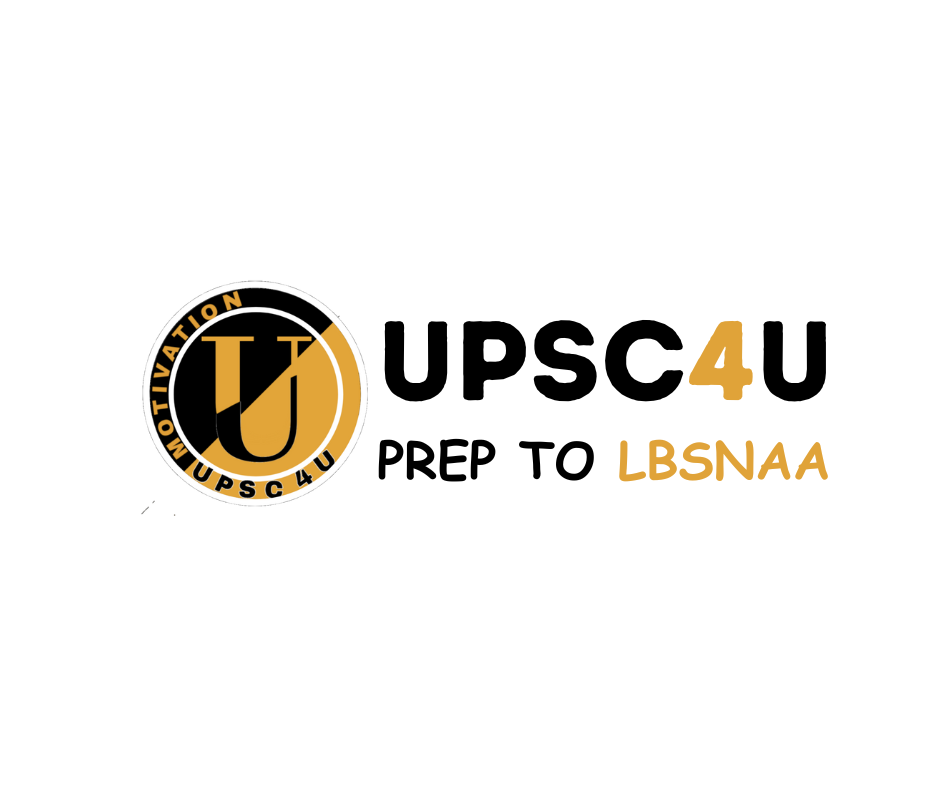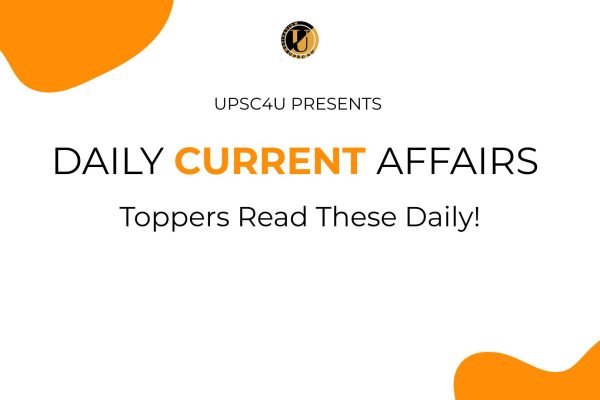THE HINDU IN HINDI:भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य विनियमन और नीतिगत कमियों के बारे में। गैर-संचारी रोग, खाद्य सुरक्षा और विनियामक ढांचे के लिए वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास जैसे विषय सीधे यूपीएससी के शासन, स्वास्थ्य और सार्वजनिक नीति पर अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडी के पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। ऐसी विनियामक आवश्यकताओं को समझना स्वास्थ्य (एसडीजी 3) और सतत उपभोग (एसडीजी 12) जैसे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से भी जोड़ा जा सकता है।
THE HINDU IN HINDI:एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव (ATNI) की रिपोर्ट
नेस्ले, कोका-कोला और हर्षे जैसे वैश्विक खाद्य निर्माताओं के 52,414 खाद्य उत्पादों का मूल्यांकन किया गया।
निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) में बेचे जाने वाले उत्पाद उच्च आय वाले देशों (HIC) की तुलना में कम स्वस्थ थे।
स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली ने इन उत्पादों के लिए 5 में से 3.5 का औसत स्कोर दिखाया।
भारत में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ
भारत गैर-संचारी रोगों (NCD) के उच्च बोझ का सामना कर रहा है, जिसमें 10.13 करोड़ भारतीय मधुमेह और मोटापे से प्रभावित हैं।
पौष्टिक भोजन की कम कीमत और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करती है।
फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की आवश्यकता
फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग उपभोक्ताओं को नमक, चीनी और वसा से भरपूर अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की पहचान करने में मदद करती है।
भारत बच्चों को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विपणन पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करने वाले विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्तावों का एक पक्ष है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत एक मसौदा अधिसूचना 2022 में पेश की गई थी, लेकिन इसमें धीमी प्रगति देखी गई है।
वैश्विक उदाहरण:
चिली और मैक्सिको जैसे देशों ने शर्करा युक्त पेय पदार्थों और अस्वास्थ्यकर स्नैक्स के लिए अनिवार्य लेबलिंग कानून अपनाए हैं।
इन उपायों ने हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करने में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं।
नीतिगत कमियाँ और सिफारिशें
कुपोषण और गैर-संचारी रोगों की उच्च दरों के बावजूद भारत में पैक के सामने लेबलिंग के लिए अनिवार्य नीतियों का अभाव है।
विशेषज्ञ सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सख्त नियामक ढाँचे की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का फोकस शिक्षा को बढ़ावा देने और वित्तीय बाधाओं को कम करने पर है, जो सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और शिक्षा सुधार जैसे विषयों के साथ संरेखित है। यह दर्शाता है कि सरकार किस तरह मध्यम आय वाले परिवारों को लक्षित कर रही है और रैंकिंग के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा दे रही है, जो यूपीएससी पाठ्यक्रम में शासन और सामाजिक क्षेत्र की पहलों के तहत प्रासंगिक है।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का शुभारंभ
6 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई।
ट्यूशन फीस और अन्य पाठ्यक्रम-संबंधी खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करता है।
पात्रता मानदंड
छात्रों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा रैंक किए गए 860 उच्च शिक्षा संस्थानों में से किसी एक में प्रवेश लेना चाहिए।
यह उन छात्रों पर लागू होता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं
स्थगन अवधि के दौरान ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट प्रदान करता है।
मध्यम आय वाले परिवारों को लक्षित करता है, जाति या अन्य सामाजिक कारकों के बावजूद निम्न आय समूहों से परे कवरेज का विस्तार करता है।
परिचालन पहलू
ऋण आवेदनों को विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाती है और सार्वजनिक और निजी बैंकों से जुड़ जाती है।
सरकार ने 2024-25 से 2030-31 तक इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे सालाना सात लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
पिछली योजनाओं से तुलना
पिछली योजनाएँ NAAC और NBA द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों तक ही सीमित थीं।
विद्यालक्ष्मी NIRF शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे पिछली योजनाओं की तुलना में पात्र संस्थानों की संख्या कम हो जाती है।
योजना के निहितार्थ
रैंकिंग महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ऋण पात्रता अब NIRF रैंकिंग पर निर्भर है।
बैंक सूची से बाहर के संस्थानों के लिए उच्च ब्याज दर वसूल सकते हैं, जिससे छात्रों की पहुँच सीमित हो सकती है।
कैरेबियाई देशों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी, आर्थिक कूटनीति, वैक्सीन कूटनीति और नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी पर जोर देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भारत की प्रवासी नीति और जलवायु परिवर्तन शमन के विषयों के साथ संरेखित है, जो इसे GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर III (जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास) के लिए प्रासंगिक बनाता है।
भारत-कैरिकॉम संबंधों को मजबूत करना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरिकॉम (कैरिबियन समुदाय) देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए सात प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव रखा।
ध्यान देने के क्षेत्रों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और विज्ञान एवं नवाचार शामिल हैं।
एसएमई क्षेत्र पर ध्यान
भारत ने पिछले शिखर सम्मेलन के दौरान कैरिकॉम क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास के लिए 1 मिलियन डॉलर के अनुदान की घोषणा की थी।
इस पहल के कार्यान्वयन पर आर्थिक सहयोग की दिशा में एक कदम के रूप में जोर दिया जा रहा है।
पांच टी को बढ़ावा देना
प्रधानमंत्री ने “पांच टी” के महत्व पर जोर दिया: व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, प्रतिभा और परंपरा।
निजी क्षेत्रों और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल की योजना बनाई गई है।
ऐतिहासिक संदर्भ
यह 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा है, जो कैरिबियन के साथ भारत की बढ़ती कूटनीतिक भागीदारी का संकेत है।
वैक्सीन कूटनीति
गुयाना के राष्ट्रपति इरफ़ान अली ने कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन पहुँचाने में भारत के सहयोग की सराहना की।
भारतीय प्रवासी और रणनीतिक हित
इस क्षेत्र में भारतीय मूल की एक महत्वपूर्ण आबादी रहती है, गुयाना में लगभग 3.2 लाख लोग रहते हैं, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मज़बूती प्रदान करते हैं।
इस चर्चा में नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में सहयोग शामिल था, जिसमें पहले प्रदान की गई 150 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का विशेष उल्लेख था।
(अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए यह महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत-चीन संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और सीमा विवादों को हल करने में विश्वास-निर्माण उपायों की भूमिका शामिल है। यह शांति-निर्माण और आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों के विषयों के साथ भी संरेखित है।
भारत-चीन आपसी विश्वास पर समझौता
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष डोंग जून ने आपसी विश्वास और समझ के पुनर्निर्माण पर काम करने पर सहमति जताई।
2020 की “दुर्भाग्यपूर्ण सीमा झड़पों” के बाद, संघर्ष के बजाय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
विघटन का पूरा होना
भारतीय और चीनी सेनाओं ने 2020 से लंबे समय तक तनाव के बाद हाल ही में पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग में विघटन पूरा किया।
इस समझौते में प्रभावित क्षेत्रों में गश्त गतिविधियों को फिर से शुरू करना शामिल था।
शांति के लिए रूपरेखा
दोनों पक्षों ने भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए भारत-चीन सीमा पर शांति और सौहार्द की आवश्यकता पर जोर दिया।
सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध आवश्यक हैं।
बैठक का संदर्भ
विंटियाने, लाओस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम-प्लस) के मौके पर चर्चा हुई।
यह सीमा विघटन के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास बनाने का एक प्रयास है।
निवारक उपायों का आह्वान: सिंह ने पुनरावृत्ति से बचने के लिए पिछली घटनाओं से सबक लेने के महत्व पर जोर दिया। दोनों राष्ट्र बातचीत और आपसी समझ के माध्यम से तनाव को कम करने का लक्ष्य रखते हैं।
THE HINDU IN HINDI:अंतर्राष्ट्रीय संगठन (यूनिसेफ), जलवायु परिवर्तन प्रभाव, सामाजिक-आर्थिक असमानता और वैश्विक जनसांख्यिकीय रुझान जैसे विषयों को कवर किया गया है। यह निबंध लेखन, नैतिकता (बाल अधिकार) और प्रारंभिक (अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट) के लिए महत्वपूर्ण है।
यूनिसेफ की SOWC-2024 रिपोर्ट अवलोकन
इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दुनिया के लगभग आधे बच्चे (लगभग 1 बिलियन) ऐसे देशों में रहते हैं जो जलवायु और पर्यावरणीय खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
बच्चों के भविष्य पर जनसांख्यिकीय बदलावों, जलवायु संकटों और तकनीकी परिवर्तनों के संयुक्त प्रभावों की जांच करता है।
पहचाने गए प्रमुख खतरे
जलवायु परिवर्तन: बढ़ता तापमान, चरम मौसम और बाढ़ बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों, खाद्य असुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाते हैं।
प्रदूषण: बच्चों के विकासशील अंगों को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिसका स्वास्थ्य और विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
जैव विविधता का ह्रास: पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करके खाद्य असुरक्षा को बढ़ाता है।
जनसांख्यिकीय बदलाव
वर्ष 2050 तक, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में वैश्विक बाल जनसंख्या के आंकड़ों में गिरावट के बावजूद सबसे बड़ी बाल आबादी होगी।
वर्ष 2050 तक अकेले भारत में 350 मिलियन से अधिक बच्चे होंगे, हालांकि यह वर्तमान संख्या की तुलना में 106 मिलियन की गिरावट दर्शाता है।
तकनीकी प्रभाव
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और नैनो प्रौद्योगिकी जैसी उभरती हुई तकनीकें बचपन के अनुभवों को बेहतर बना सकती हैं।
हालाँकि, डिजिटलीकरण शोषण, दुर्व्यवहार के जोखिम को बढ़ाता है और सीमित डिजिटल पहुँच वाले क्षेत्रों में असमानता को बढ़ाता है।
बुनियादी ढाँचे की असमानता
कम आय वाले देशों में से 26% से भी कम देशों में विश्वसनीय इंटरनेट पहुँच है, जबकि उच्च आय वाले क्षेत्रों में यह 95% है।
अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी अधिकारों तक पहुँच को सीमित करता है।
खाद्य सुरक्षा के लिए निहितार्थ:
कृषि में जलवायु संबंधी व्यवधान कुपोषण और गरीबी के जोखिम को बढ़ाते हैं, जो बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।
कार्रवाई का आह्वान
जलवायु-लचीले बुनियादी ढाँचे और शिक्षा प्रणालियों में निवेश।
भविष्य की पीढ़ियों के लिए समान प्रौद्योगिकी पहुँच और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करें।
जैव प्रौद्योगिकी, संधारणीय कृषि, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रभाव आकलन सहित। यह कृषि में प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी नैतिक चिंताओं पर निबंध विषयों के लिए भी प्रासंगिक है। भारत में खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए जीएम फसल नीति और उसके निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है।
जी.एम. फसलों का परिचय
आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी.एम.) फसलों को कीट प्रतिरोध और शाकनाशी सहिष्णुता जैसे गुणों को शामिल करने के लिए इंजीनियर किया जाता है।
CRISPR जैसे उपकरण पौधे के जीनोम में लक्षित परिवर्तन करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे लागत कम होती है और स्वीकृति बढ़ती है।
जी.एम. फसलों के लाभ
बढ़ी हुई उपज: बीटी कपास और एच.टी. फसलों जैसी जी.एम. फसलें कीटों और खरपतवारों से होने वाले नुकसान को कम करके उच्च उत्पादकता को सक्षम बनाती हैं।
कीट प्रतिरोध: बीटी फसलें ऐसे विष उत्पन्न करती हैं जो विशिष्ट कीटों को मारते हैं, जिससे कीटनाशकों का उपयोग कम होता है।
पोषण संवर्धन: कुछ जी.एम. फसलों को उच्च पोषण सामग्री के लिए इंजीनियर किया जा सकता है।
वनों की कटाई में कमी: उच्च उत्पादकता कृषि भूमि के विस्तार की आवश्यकता को कम कर सकती है।
जी.एम. फसलों के साथ चुनौतियाँ
पर्यावरणीय प्रभाव
ग्लाइफोसेट जैसे शाकनाशियों पर अत्यधिक निर्भरता ने खरपतवारों में प्रतिरोध को जन्म दिया है।
एकल कृषि प्रथाओं के कारण जैव विविधता में कमी।
स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: जी.एम. फसलों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर सीमित डेटा।
विनियमन और विकास लागत: विनियमन की उच्च लागत छोटे संगठनों को जीएम फसलें विकसित करने से रोकती है।
कृषि प्रबंधन संबंधी चिंताएँ
जीएम फसलों को अपनाने के लिए प्रतिरोध को रोकने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फसल चक्र जैसे कृषि पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है।
फसल के प्रकारों में विविधता की कमी से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है।
लाभ-संचालित मॉडल:
निजी निगमों द्वारा जीएम फसलों का विकास अक्सर पारिस्थितिक संतुलन पर लाभ को प्राथमिकता देता है।
पेटेंट की गई जीएम तकनीक के लिए लाइसेंसिंग लागत किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ाती है।
भारत में नीति और कानूनी ढाँचा
जीएम फसल अनुमोदन को विनियमित करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जीईएसी अनुमोदन के बावजूद जीएम सरसों को विनियामक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा।
भविष्य की संभावनाएँ
अनुसंधान और विकास: सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान में निवेश लागत को कम कर सकता है और जीएम तकनीक को छोटे खिलाड़ियों के लिए सुलभ बना सकता है।
एकीकृत कीट प्रबंधन: जीएम फसलों को पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ मिलाने से जोखिम कम हो सकते हैं।
स्थिरता पर ध्यान: नीतियों में फसल चक्र, विविध खेती, तथा रासायनिक खरपतवारनाशकों पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
(अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और पेपर III (आर्थिक विकास) में राजनीतिक सुधार, आर्थिक संकट और शासन के विषयों के लिए प्रासंगिक है। यह आर्थिक संकटों से राजनीतिक बदलाव कैसे उत्पन्न होते हैं, पहचान की राजनीति की भूमिका और क्षेत्रीय स्थिरता और शासन के लिए निहितार्थों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
श्रीलंका में चुनावी बदलाव: अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पावर (NPP) पार्टी ने श्रीलंका के संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल की, जो पारंपरिक राजनीतिक गतिशीलता से एक महत्वपूर्ण बदलाव था।
स्थापित राजनीतिक दलों का पतन: श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (SLFP) और यूनाइटेड नेशनल पार्टी (UNP) जैसी स्थापित पार्टियों को नाटकीय चुनावी हार का सामना करना पड़ा। राजपक्षे जैसे पूर्व में प्रभावशाली परिवारों को हाशिये पर धकेल दिया गया।
तमिल राजनीतिक बदलाव: उत्तरी प्रांतों में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली तमिल राष्ट्रवादी दलों में गिरावट आई। NPP ने पारंपरिक रूप से तमिल पार्टियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में बढ़त हासिल की, जो एक प्रमुख राजनीतिक बदलाव था।
उत्प्रेरक के रूप में आर्थिक संकट: स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका का सबसे खराब आर्थिक संकट, जिसमें बाहरी ऋण मुद्दे, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति शामिल हैं, ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को खारिज करने में योगदान दिया।
ऐतिहासिक समानता: यह चुनाव श्रीलंका के 1977 के बदलाव से तुलना करता है, जिसने नवउदारवादी आर्थिक सुधारों और एक मजबूत कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शुरुआत की।
प्रतिनिधित्व और लिंग: नई संसद में विविध प्रतिनिधित्व शामिल है, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों की महिलाओं को सीटें मिली हैं, जो अभिजात वर्ग के वर्चस्व वाली राजनीति से अलग होने को दर्शाता है।
आगे की चुनौतियाँ: एनपीपी को जातीय शिकायतों, आर्थिक असमानता को दूर करने और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए श्रीलंका के बाहरी ऋण को पुनर्गठित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ: श्रीलंका का बदलाव लेनदारों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने, आईएमएफ द्वारा संचालित सुधारों को लागू करने और क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक दबावों का जवाब देने की आवश्यकता को दर्शाता है।
THE HINDU IN HINDI:भारत के व्यापारिक निर्यात और आयात, अर्थव्यवस्था द्वारा सामना किए जाने वाले हाल के रुझानों और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। इन गतिशीलता को समझना GS 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था अनुभाग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यापार, भुगतान संतुलन और आर्थिक विकास से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है।
निर्यात में मौजूदा रुझान
अक्टूबर में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 17.25% की वृद्धि देखी गई, जो वर्ष के दूसरे सबसे अधिक निर्यात आँकड़ों में $39.2 बिलियन का योगदान देता है।
इस वर्ष अब तक कुल निर्यात वृद्धि सुस्त बनी हुई है, जिसमें संचयी वृद्धि केवल 1% रही है।
गैर-पेट्रोलियम निर्यात ने अक्टूबर में 25.6% की वृद्धि के साथ उछाल का नेतृत्व किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों के लिए $211.3 बिलियन तक पहुँच गया।
पेट्रोलियम क्षेत्र का विश्लेषण
अक्टूबर में भारत का तेल आयात 13.2% बढ़कर $18.3 बिलियन तक पहुँच गया, जबकि पेट्रोलियम निर्यात 22% से अधिक गिरकर $4.6 बिलियन के तीन साल के निचले स्तर पर पहुँच गया।
तेल व्यापार घाटा रिकॉर्ड $13.7 बिलियन तक पहुँच गया।
बढ़ता व्यापार घाटा
अक्टूबर में कुल व्यापार घाटा बढ़कर $66.3 बिलियन हो गया, जो अब तक का दूसरा सबसे उच्च स्तर है, जो उच्च सोने के आयात और तेल की कीमतों के कारण है।
शादी के मौसम में मौसमी मांग के कारण सोने का आयात उच्च बना हुआ है।
वैश्विक व्यापार चुनौतियाँ
विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने 2025 में वैश्विक व्यापार वृद्धि को 3% पर अनुमानित किया है, जो 2024 में 2.7% से थोड़ा अधिक है, जो धीमी वैश्विक रिकवरी को दर्शाता है।
चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव व्यापार में अनिश्चितता को बढ़ाते हैं।
अमेरिकी व्यापार नीतियों का प्रभाव
डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में आने वाले अमेरिकी प्रशासन से टैरिफ और घरेलू उत्पादन प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के व्यापार को प्रभावित कर सकता है।
भारत को अपने नीतिगत निर्णयों, जैसे कि अपडेट किए गए लैपटॉप आयात प्रबंधन प्रणाली के बारे में सतर्क रहना चाहिए, ताकि अमेरिकी प्रशासन का अनावश्यक ध्यान आकर्षित न हो।
THE HINDU IN HINDI:विदेशी मुद्रा भंडार
व्यापार घाटे के बढ़ने के बावजूद, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आरामदायक बना हुआ है, जो एक साल के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।