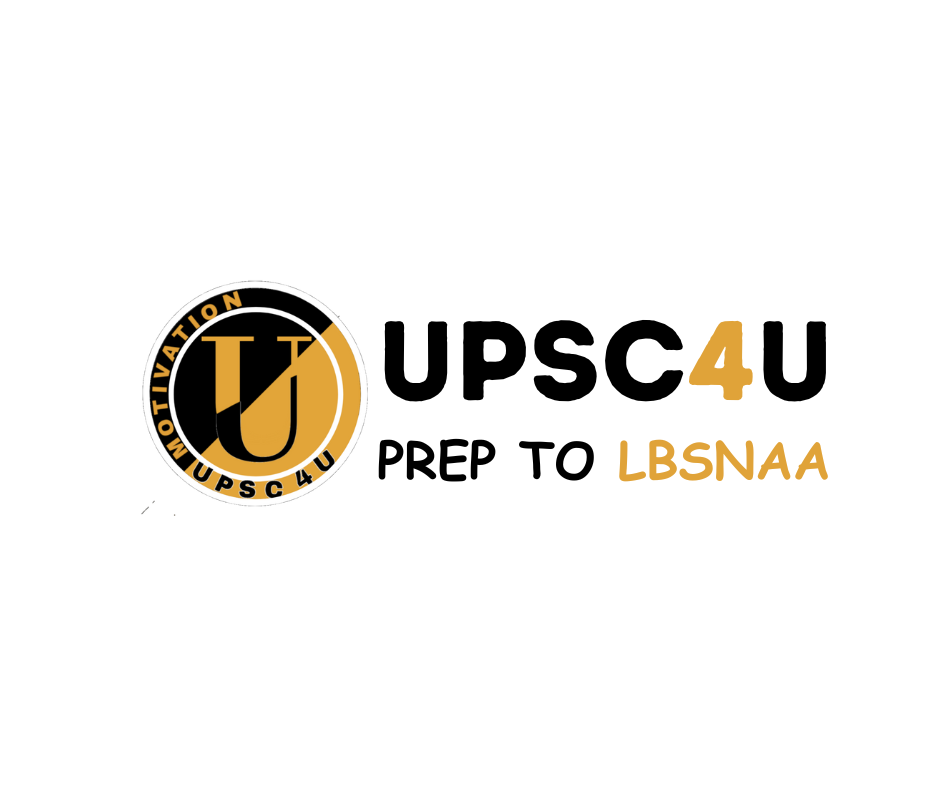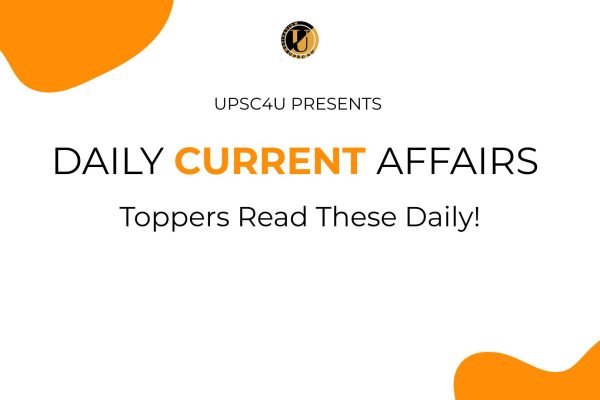आज की 4 अगस्त, 2025 की द हिंदू समाचार पत्र और संपादकीय विश्लेषण से आपके लिए महत्वपूर्ण सुर्खियाँ लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होंगी। यह लेख विभिन्न महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर गहन जानकारी प्रदान करता है, जिसे आपके Prelims और Mains दोनों के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। आज का सत्र एक संपूर्ण करेंट अफेयर्स पैकेज है, जिसमें द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, और अन्य महत्वपूर्ण स्रोत शामिल हैं।
चलिए, आज के मुख्य विषयों पर एक नज़र डालते हैं:
1. मिथुन (ग्याल): संरक्षण की पुकार
यह प्रजाति हाल ही में चर्चा में रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के वैज्ञानिक और किसान केंद्र सरकार से मिथुन को राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) के तहत शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
- परिचय: मिथुन, जिसे आमतौर पर ग्याल भी कहते हैं, भारत में पाई जाने वाली एक अर्ध-पालतू (semi-domesticated) बोवाइन प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस (Bos frontalis) है। यह भारतीय बाइसन ‘गौर’ का एक छोटा संस्करण है और इसे ‘पहाड़ों का मवेशी’ (Cattle of the Mountain) भी कहा जाता है।
- महत्व: अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का यह राजकीय पशु (State Animal) है। अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजातियों द्वारा सोलुंग महोत्सव (Solung Festival) मिथुन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
- निवास स्थान: यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम), म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों (tropical rain forests) में पाया जाता है।
- संरक्षण स्थिति:
- IUCN रेड लिस्ट: अतिसंवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध है, जो इसकी घटती जनसंख्या को दर्शाता है.
- CITES: परिशिष्ट I (Appendix I) में है, जिसका अर्थ है कि इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है.
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: वर्तमान में यह अधिनियम के किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं है, और वैज्ञानिक तथा किसान इसी अधिनियम के तहत इसे अनुसूची I (Schedule I) में शामिल करने की मांग कर रहे हैं ताकि इसे उच्च सुरक्षा मिल सके.
- खाद्य पशु का दर्जा: सितंबर 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मिथुन को खाद्य पशु (Food Animal) के रूप में मान्यता दी है।
- एम-मित्रा ऐप (M-Mithra App): यह ऐप मिथुन पालकों को अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किया गया है।
2. ओरेश्निक मिसाइल: रूस की नई हाइपरसोनिक शक्ति
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस की नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल (hypersonic ballistic missile), ओरेश्निक (Oreshnik), अब ऑपरेशनल हो चुकी है और इसे बेलारूस में तैनात किया जाएगा।
- विशेषताएँ:
- यह ध्वनि की गति से पाँच गुना से अधिक (Mach 5 से अधिक) तेज़ी से उड़ान भरने में सक्षम है, इसकी गति मैक 10 (Mach 10) से भी अधिक है।
- इसकी रेंज 5000 किमी है।
- यह ठोस ईंधन (solid fuel) प्रणाली का उपयोग करती है, जिससे इसे तेज़ी से लॉन्च और आसानी से परिवहन किया जा सकता है।
- इसमें एमआईआरवी (MIRV) टेक्नोलॉजी (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल्स) का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को भेद सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित किया जा सकता है।
- यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वॉरहेड्स (Nuclear and Conventional Warheads) ले जाने में सक्षम है।
- इसे पहली बार 12 नवंबर, 2024 को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था।
- रणनीतिक महत्व: यह नाटो समूह और पश्चिमी देशों से निपटने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
- UPSC संदर्भ: रक्षा और सुरक्षा (GS Paper 3) के लिए महत्वपूर्ण।
3. आईएनएस सतपुड़ा: भारतीय नौसेना का बहु-भूमिका वाला युद्धपोत
आईएनएस सतपुड़ा हाल ही में सिंगापुर पहुंचा है ताकि वहाँ एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले सके।
- परिचय: आईएनएस सतपुड़ा भारतीय नौसेना का एक स्टील्थ मल्टी-रोल युद्धपोत (stealth multi-role warship) है।
- श्रेणी: यह शिवालिक श्रेणी (Shivalik Class) का जहाज है और इसे प्रोजेक्ट 17 (Project 17) के तहत तैयार किया गया है। शिवालिक श्रेणी के जहाजों का नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखा गया है, और सतपुड़ा का नाम भी सतपुड़ा पहाड़ियों पर है।
- क्षमताएँ: यह मल्टी-रोल ऑपरेशन (multi-role operation) चला सकता है, जिसमें हवाई-रोधी, सतह-रोधी, और पनडुब्बी-रोधी युद्ध शामिल हैं।
- निर्माण: इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) ने बनाया है।
- कमीशन: इसे 20 अगस्त, 2011 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- मेक इन इंडिया: यह भारत के मेक इन इंडिया (Make in India) पहल को बढ़ावा देता है क्योंकि इसे पूरी तरह से भारत में बनाया गया है।
- UPSC संदर्भ: रक्षा और सुरक्षा (GS Paper 3) के लिए महत्वपूर्ण।
4. रेड पांडा: पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक
सिक्किम के हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लगभग 7 साल बाद रेड पांडा के शावकों का जन्म हुआ है, जिससे यह प्रजाति फिर से सुर्खियों में है।
- परिचय: रेड पांडा को लेसर पांडा (Lesser Panda) या फायरफॉक्स (Firefox) भी कहा जाता है। यह एक वृक्षवासी (Arboreal) प्रजाति है (जो पेड़ों पर रहती है) और मुख्य रूप से शाकाहारी होती है, हालांकि कभी-कभी छोटे कीड़े भी खाती है।
- निवास स्थान: यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, विशेषकर भारत (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम), नेपाल, भूटान, म्यांमार और दक्षिणी चीन में। सिक्किम का यह राजकीय पशु (State Animal) भी है।
- संरक्षण स्थिति:
- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध है।
- CITES: परिशिष्ट I (Appendix I) में है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I (Schedule I) में है, जो इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है।
- मुख्य खतरा: वनों की कटाई और आवास का नुकसान इसकी आबादी के लिए मुख्य खतरा हैं।
- सूचक प्रजाति (Indicator Species): रेड पांडा एक सूचक प्रजाति है। ये प्रजातियाँ हमें बताती हैं कि जिस क्षेत्र में वे मौजूद हैं, वहाँ का पर्यावरण स्वस्थ है या नहीं। यदि रेड पांडा संकट में हैं, तो यह हिमालयी वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी संकेत है।
- UPSC संदर्भ: पर्यावरण और जैव विविधता (GS Paper 3) के लिए महत्वपूर्ण।
5. इंडो-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल (IBRRI)
रामसर कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP15) की एक बैठक के दौरान इंडो-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल (Indo-Burma Ramsar Regional Initiative – IBRRI) पर चर्चा हुई।
- उद्देश्य: यह पहल वेटलैंड्स (आद्रभूमि) के संरक्षण और बहाली के लिए एक क्षेत्रीय सहयोग है।
- सदस्य देश: इसमें पाँच दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं – कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। भारत इसमें शामिल नहीं है।
- प्रबंधन: इसका प्रबंधन एक स्टीयरिंग कमेटी और IUCN एशिया ऑफिस (IUCN Asia Office) द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है।
- सहयोग: इसे IUCN के ब्रिज प्रोजेक्ट (IUCN’s Bridge Project) का समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य सीमा पार नदियों और वेटलैंड्स पर देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
- रणनीतिक योजना: IBRRI की 2025 से 2030 तक की रणनीतिक योजना है, जिसमें वेटलैंड्स के संरक्षण और बहाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- UPSC संदर्भ: पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय संबंध (GS Paper 3 और 2) के लिए महत्वपूर्ण।
6. डीनोटिफाइड जनजातियाँ: स्थायी राष्ट्रीय आयोग की मांग
हाल ही में डीनोटिफाइड जनजातियों (Denotified Tribes – DNTs) के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग (Permanent National Commission) स्थापित करने की तीव्र मांग उठी है।
- परिचय: डीनोटिफाइड जनजातियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 (Criminal Tribes Act, 1871) के तहत ‘आपराधिक जनजाति’ का लेबल दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद, यह अधिनियम 1952 में निरस्त कर दिया गया, और इन जनजातियों को ‘डीनोटिफाइड’ (विमुक्त) किया गया।
- चुनौतियाँ: इन समुदायों को भूमिहीनता, सरकारी योजनाओं से बहिष्करण, सामाजिक भेदभाव, उच्च गरीबी दर और कम साक्षरता दर जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हें संवैधानिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है।
- महत्वपूर्ण आयोग:
- रेणके आयोग (Renke Commission): 2008 में स्थापित, जिसने DNTs को पहचान दिलाने की दिशा में पहला प्रयास किया।
- इदते आयोग (Idate Commission): भीखू रामजी इदते जी की अध्यक्षता में 2014 में स्थापित, जिसने DNTs के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग बनाने की सिफारिश की थी।
- SEED योजना: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई SEED (Scheme for Economic Empowerment of DNTs) योजना DNTs, नोमेडिक और सेमी-नोमेडिक जनजातियों को मुफ्त कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका विकास प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता: भारत की लगभग 10% आबादी DNTs, नोमेडिक और सेमी-नोमेडिक जनजातियों की है। एक आयोग इन समुदायों के लिए दीर्घकालिक नीतियाँ बनाने, कानूनी सहायता प्रदान करने और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करने में मदद करेगा, जिससे ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जा सके।
- UPSC संदर्भ: सामाजिक न्याय और नीति (GS Paper 2) के लिए महत्वपूर्ण।
7. बायोसिमिलर ड्रग्स: भारत में सरलीकरण की आवश्यकता
एक हालिया लेख में चर्चा की गई है कि यूके और यूएस की तरह, भारत को भी बायोसिमिलर दवाओं के परीक्षण दिशानिर्देशों को सरल बनाना चाहिए ताकि वे अधिक किफायती और सुलभ बन सकें।
- जेनेरिक मेडिसिन (Generic Medicines): ये सरल रासायनिक संरचना वाली दवाएं होती हैं, जिनकी कॉपी करना आसान होता है। पेटेंट समाप्त होने के बाद इन्हें मूल दवा की नकल करके बनाया जाता है, इसलिए ये सस्ती होती हैं।
- बायोलॉजिक्स (Biologics): ये बड़ी और जटिल दवाएं होती हैं, जो जीवित कोशिकाओं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से बनती हैं। इन्हें कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है。
- बायोसिमिलर्स (Biosimilars): ये बायोलॉजिक्स की कॉपी होती हैं। इन्हें बनाना जेनेरिक दवाओं की तुलना में अधिक जटिल और महंगा होता है, क्योंकि इन्हें जानवरों पर और क्लिनिकल परीक्षणों के माध्यम से अपनी सुरक्षा और प्रभावशीलता साबित करनी होती है。
- चुनौती: भारत में बायोसिमिलर बहुत महंगे हैं, क्योंकि यहाँ के नियम सख्त हैं और परीक्षण प्रक्रियाएँ जटिल हैं। यूके और यूएस ने इन परीक्षण मानदंडों को आसान बनाया है।
- आवश्यकता: सरल परीक्षण मानदंड बायोसिमिलर की लागत को कम करेंगे, जिससे जीवन रक्षक दवाएं अधिक रोगियों के लिए वहनीय बनेंगी।
- UPSC संदर्भ: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य (GS Paper 3 और 2) के लिए महत्वपूर्ण।
8. आलू और टमाटर का साझा पूर्वज
एक हालिया वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि आलू और टमाटर दोनों एक ही सामान्य पूर्वज साझा करते हैं।
- शोध का निष्कर्ष: लगभग 9 मिलियन वर्ष पहले, जंगली टमाटरों को एक पौधे, जिसका नाम यूटोबेरोसम (Utoberosum) है, के साथ संकरित किया गया था, जिससे आधुनिक आलू विकसित हुए।
- आनुवंशिक संबंध: आज के आधुनिक आलू के 40% जीन टमाटर से और 60% जीन यूटोबेरोसम से आते हैं।
- महत्व: यह शोध आलू के विकास और इसकी किसी भी पर्यावरण में जीवित रहने की क्षमता को समझने में मदद करता है।
- UPSC संदर्भ: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (GS Paper 3) के लिए महत्वपूर्ण।
9. नांगरनी स्पर्धा: महाराष्ट्र की पारंपरिक बैल दौड़
नांगरनी स्पर्धा महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली एक सदियों पुरानी बैल दौड़ (Ox race) है, जो हाल ही में सुर्खियों में रही।
- परिचय: यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मानसून के मौसम में आयोजित की जाती है।
- सांस्कृतिक महत्व: यह किसानों और उनके बैलों के बीच के बंधन, बैल की ताकत और गति, और किसान के कौशल का उत्सव है。 यह महाराष्ट्र की ग्रामीण जीवन और कृषि विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है。
- दौड़ की विशेषताएँ: यह दौड़ कीचड़ भरे ट्रैक पर होती है, जहाँ किसान नंगे पैर चलते हैं। बैलों को सजाया जाता है और उनके सींगों को रंगा जाता है。
- समान आयोजन: भारत में इसी तरह के अन्य आयोजन भी होते हैं:
- कंबाला (Kambala): कर्नाटक में भैंसों की दौड़।
- मरमड़ी (Maramadi): केरल में बैल दौड़ की एक समान शैली।
- UPSC संदर्भ: कला और संस्कृति (GS Paper 1) के लिए महत्वपूर्ण।
10. राइट टू रिपेयर (मरम्मत का अधिकार): मानव ज्ञान की सुरक्षा
आज के संपादकीय में ‘राइट टू रिपेयर’ (Right to Repair) आंदोलन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि यह केवल उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों के अंतर्निहित ज्ञान (tacit knowledge) की सुरक्षा भी है।
- राइट टू रिपेयर: यह एक ऐसा विचार है जहाँ उपभोक्ताओं (जैसे आप और मैं) को अपने उत्पादों की आसानी से मरम्मत करने का अधिकार होता है। इसके लिए कंपनियों को डिवाइस के पार्ट्स, मैनुअल और सॉफ्टवेयर अपडेट आसानी से उपलब्ध कराने चाहिए।
- ई-वेस्ट (E-Waste): यदि मरम्मत का अधिकार नहीं मिलता है, तो उत्पाद फेंक दिए जाते हैं, जिससे ई-कचरा बढ़ता है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक है।
- अंतर्निहित ज्ञान (Tacit Knowledge): यह वह कौशल और अनुभव है जो लोग काम करके, अभ्यास करके और प्रयोग करके सीखते हैं, न कि किताबों या कोड से। भारत में ऐसे कई स्थानीय मरम्मतकर्ता हैं जिनके पास यह विशेषज्ञता है।
- चुनौती: नई गैजेट्स को मरम्मत करना मुश्किल हो रहा है, और कंपनियाँ स्थानीय मरम्मतकर्ताओं के कौशल को पीछे छोड़ना चाहती हैं।
- सुझाव: लेखक का तर्क है कि सरकार और टेक कंपनियों को मरम्मत कार्य को एक ज्ञान-आधारित कार्य के रूप में मान्यता देनी चाहिए। स्थानीय तकनीशियनों को सरकारी योजनाओं जैसे ई-श्रम योजना (eShram Scheme) या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) के तहत समर्थन दिया जाना चाहिए।
- निष्कर्ष: ‘राइट टू रिपेयर’ टूटी हुई चीज़ों को ठीक करने से कहीं ज़्यादा है; यह मरम्मतकर्ताओं के पारंपरिक ज्ञान और कौशल प्रणाली को संरक्षित करने और समर्थन करने के बारे में भी है।
- UPSC संदर्भ: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और नीति (GS Paper 3 और 2) के लिए महत्वपूर्ण।
UPSC तैयारी के लिए सुझाव:
- Prelims अभ्यास प्रश्न: हर लेख के बाद दिए गए Prelims प्रश्नों को हल करें। यह आपकी याद रखने की क्षमता और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- Mains उत्तर लेखन: राइट टू रिपेयर पर दिए गए Mains प्रश्न का उत्तर लिखने का अभ्यास करें। उत्तर संरचना के लिए दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें (परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष)। अपने उत्तरों को टेलीग्राम पर Deepak Yadav Education Mains Group में साझा कर सकते हैं और दूसरों के उत्तरों की समीक्षा भी कर सकते हैं.
- व्यापक कवरेज: आज का सत्र करंट अफेयर्स का एक पूर्ण पैकेज है। इसे अच्छे से पढ़ें और इसके अलावा कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं है।
- संसाधन: इस लेक्चर की हाई-क्वालिटी PDF (हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) के लिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यह एक बार का निवेश है, और यह आपको सभी पुराने और नए पीडीएफ तक आजीवन पहुंच प्रदान करेगा।
हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपकी UPSC तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें