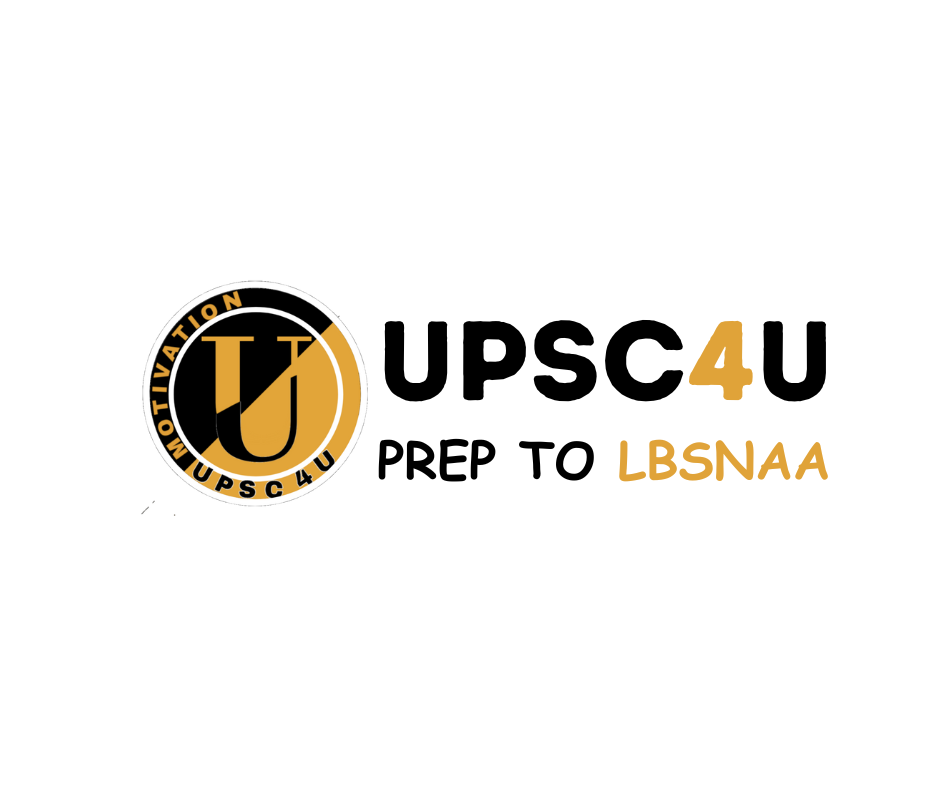| दृष्टिकोण: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 की पृष्ठभूमि और प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।42वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख परिवर्तनों पर प्रकाश डालिये। संवैधानिक ढाँचे पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की चर्चा कीजिये। बाद में हुए उलटफेर और संशोधनों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।उचित निष्कर्ष दीजिये। |
परिचय:
42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन था, आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य सत्ता को केंद्रीकृत करना, न्यायिक निगरानी को कम करना और भारतीय संविधान में कई बदलाव करना था। इस संशोधन को प्रायः ‘मिनी-संविधान’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा।
मुख्य भाग:
42वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख परिवर्तन:
- सत्ता का केंद्रीकरण:
- निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) को सुदृढ़ किया गया: संघर्ष के मामलों में DPSP को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ बनाया गया।
- न्यायपालिका पर प्रतिबंध: अनुच्छेद 32, 131, 226 और 368 में संशोधनों ने कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अधिकार को सीमित कर दिया, जिससे विधायी मामलों में न्यायिक भागीदारी सीमित हो गई।
- केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि: इसने शिक्षा, वन, वन्य पशु और पक्षियों का संरक्षण तथा माप-तौल जैसे प्रमुख विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया।
- संसद की भूमिका को सुदृढ़ बनाना:
- संसद और राज्य विधानसभाओं का विस्तारित कार्यकाल:
- कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
- उदाहरण: पाँचवीं लोकसभा (वर्ष 1971-77) को इस प्रावधान से लाभ मिला।
- न्यायिक समीक्षा से कुछ कानूनों का संरक्षण:
- अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कुछ DPSP को लागू करने के लिये बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- संसद और राज्य विधानसभाओं का विस्तारित कार्यकाल:
- मौलिक कर्त्तव्यों का परिचय: संविधान में भाग IVA (अनुच्छेद 51A) जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिये 10 मौलिक कर्त्तव्यों को शामिल किया गया।
- प्रस्तावना संशोधन: प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
- संस्थागत परिवर्तन: इसके परिणामस्वरूप नियमित न्यायालयों के बाहर सेवा विवादों को निपटाने के लिये प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन किया गया।
संवैधानिक संरचना पर प्रभाव:
- सकारात्मक:
- मौलिक कर्त्तव्यों की मान्यता: मौलिक कर्त्तव्यों की शुरुआत ने नागरिकों में ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया और उनके अधिकारों को बढ़ाया।
- प्रस्तावना संवर्द्धन: ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ को जोड़ने से समावेशी, समतापूर्ण तथा एकजुट भारत की संवैधानिक दृष्टि स्पष्ट हुई।
- प्रशासनिक दक्षता: प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्माण से नियमित न्यायालयों पर बोझ कम करने में मदद मिली, जिससे सेवा विवादों के तेज़ी से समाधान को बढ़ावा मिला।
- नकारात्मक:
- संघवाद का परिवर्तन: संघवाद के परिवर्तन से राज्य की स्वायत्तता कम हो गई, जिससे भारत एकात्मक पूर्वाग्रह की ओर बढ़ गया।
- शिक्षा जैसे राज्य-विषयों पर केंद्र के प्रभुत्व ने सहकारी संघवाद को कमज़ोर कर दिया।
- मौलिक अधिकारों का कमज़ोर होना: न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की भूमिका कमज़ोर हो गई।
- केशवानंद भारती मामले (वर्ष 1973) को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था, जिसे बाद में संशोधनों द्वारा बहाल कर दिया गया।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों की बढ़ी हुई भूमिका: शहरी भूमि सीमा अधिनियम (वर्ष 1976) जैसे कानूनों को अनुच्छेद 31C के तहत संरक्षण दिया गया।
- संघवाद का परिवर्तन: संघवाद के परिवर्तन से राज्य की स्वायत्तता कम हो गई, जिससे भारत एकात्मक पूर्वाग्रह की ओर बढ़ गया।
निष्कर्ष:
42वाँ संशोधन, हालाँकि अपने दायरे में महत्त्वाकांक्षी था, लेकिन संविधान के लोकतांत्रिक और संघीय चरित्र को कमज़ोर करने के कारण इसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालाँकि मौलिक कर्त्तव्यों और कल्याणकारी राज्य पर ज़ोर जैसे कुछ प्रावधान प्रभावशाली बने हुए हैं, लेकिन बाद में 44वें संशोधन ने संतुलन बहाल किया।