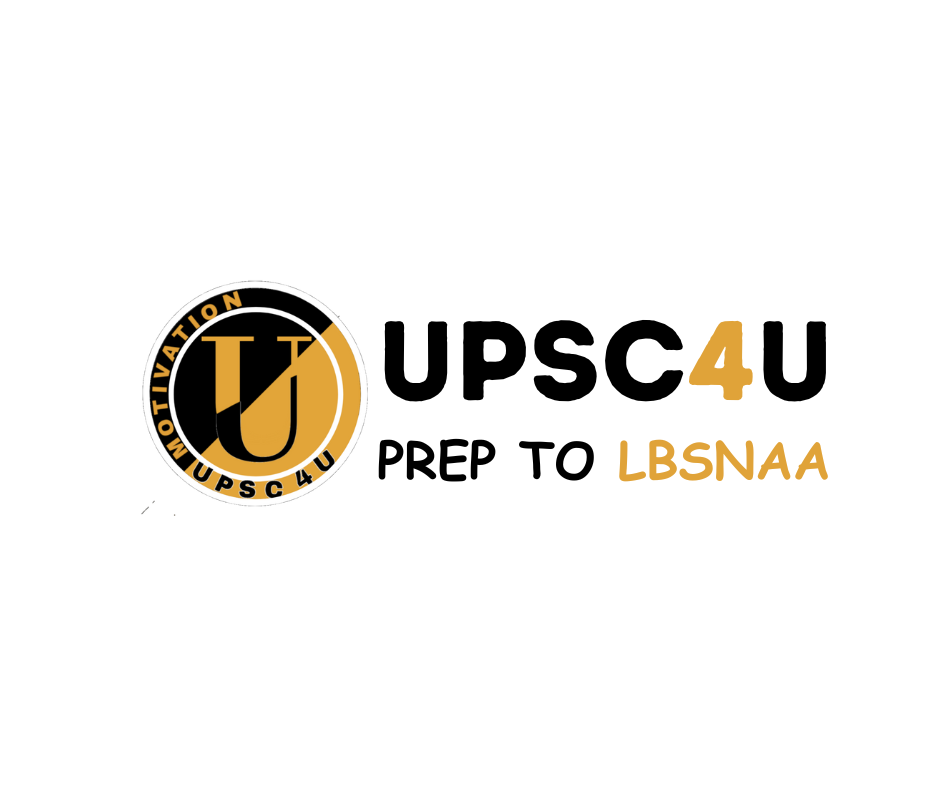भू-आकृति विज्ञान
पृथ्वी की उत्पत्ति व भूगार्भिक इतिहास
- पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्त-ए-बफन द्वारा 1749 ई. में किया गया।
- पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में 2 प्रकार की संकल्पनाएं दी गयीं-
- अद्वैतवादी परिकल्पना
- द्वैतवादी परिकल्पना
- अद्वैतवादी परिकल्पना में कांट की गैसीय परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का वर्णन किया गया है।
- द्वैतवादी संकल्पना में चैम्बरलिन व् मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जींस (1919 ई.) व जेफ्रीज (1921 ई.) की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में बताया गया है।
पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास
- रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आयु की सबसे विश्वसनीय व्याख्या नहीं हो सकी है। इन पदार्थों के अध्ययन के आधर पर पियरे क्यूरी एवं रदरफोर्ड ने पृथ्वी की आयु को 2-3 अरब वर्ष अनुमानित की है।
- आदी कल्प की चट्टानों में ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता है। इन शैलों में जीवाश्मों का पुर्णतः आभाव है। इनमें सोना तथा लोहा पाया जाता है, भारत में प्री-कैम्ब्रियन कल में अरावली पर्वत व् धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ था।
- प्राचीनतम अवसादी शैलों एवं विन्ध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन कल में हुआ।
- अप्लेशियन पर्वतमाला का निर्माण आर्डोविसियन काल में हुआ।
- पर्मियन युग में हर्सीनियन पर्वतीकरण हुए जिनसे स्पेनिश मेसेटा, वोस्जेस, ब्लैक फारेस्ट, अल्लवाई, विएनशान जैसे पर्वत निर्मित हुए।
- ट्रियासिक काल को रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है, गोंडवाना लैण्ड भूखंड का विभाजन इसी कल में हुआ, जिससे अक्रिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत तथा दक्षिणी अमेरिका के ठोस स्थल बने।
- कृटेशियन काल में एंजियोस्पर्म पौधों का विकास प्रारंभ हुआ। इसी काल में भारत के पठारी भागों में लावा का दरारी उदभेदन हुआ।
- सनोजोइक काल को टर्शियरी युग भी कहा जाता है।
| भूगर्भ की प्रमुख असम्बद्धताएं | ||
| असम्बद्धताएं | स्थिति (लगभग) | गहराई (किमी.) |
| कोनार्ड असम्बद्धता | वाह्य एवं आतंरिक भूपटल के मध्य | – |
| मोहो असम्बद्धता | भूपटल एवं मेंटल के मध्य | 30-35 |
| रेपेटी असम्बद्धता | वाह्य एवं आतंरिक मेंटल के मध्य | 700 |
| गुटेबर्ग-बाइचर्ट | मेंटल एवं कोर के मध्य | 2900 |
| लेहमैन असम्बद्धता | आतंरिक तथा वाह्य कोर के मध्य | 500 |
| पृथ्वी की विभिन्न परतों का संघटन एवं भौतिक गुण | ||||
| परतें | सापेक्षिक घनत्व | गहराई | तत्व | भौतिक गुण |
| बहरी सियाल | 2.75-2.90 | 1. महाद्वीप के नीचे ६० किमी. तक2. अटलांटिक महासागर के नीचे 29 किमी तक3. प्रशांत महासागर के नीचे अत्यल्प गहराई तक | मुख्य रूप से सिलिका और अल्युमिनियम तथा अन्य तत्व ऑक्सीजन, पोटैशियम, मैग्नीशियम | ठोस |
| भीतरी सियाल परत | 4.75 | 1. 60 किमी. गहराई तक2. 60-1200 किमी. गहराई तक | मुख्यतः सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्सियम, अल्युमिनियम, पोटैशियम, सोडियम | प्लास्टिक नुमा |
| मिश्रित परत | 4.75-5.0, सीमा की उपरी अर्द्ध ठोस तथा निचली ठोस परत का मिश्रण | 1200-2900 किमी. | ऑक्सीजन, सिलिका मैग्नीशियम, लोहे का भरी मिश्रण तथा निकिल | प्लास्टिक नुमा |
| केन्द्रक | 7.8-11.0 | 2900-6378 | निकिल तथा लोहा | ठोस या तरल |
- उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति नवजीवी महाकल्प में हुई।
- पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आगमन प्लीस्टोसीन काल में हुआ तथा मानव एवं स्तनपायी जीव इसी कल में विकसित हुए।
- 1921 में अल्फ्रेड वेगनर ने सम्पूर्ण विश्व की जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या को सुलझाने के लिए अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग तक सम्पूर्ण महाद्वीप एक में मिले हुए थे, जिसे इन्होंने पैन्जिया नाम दिया।
- 1926 में हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया।
- भू-पटल और उसके नीचे की अनुपटल को सम्मिलित रूप से स्थल खंड कहलाते हैं। 7 बड़ी एवं 20 छोटी भू-प्लेटों में विभक्त हैं। पृथ्वी के स्थलमंडल की मुख्य प्लेटें इस प्रकार हैं-
- यूरेशियन प्लेट
- इन्डियन प्लेट
- अफ़्रीकी प्लेट
- अमेरिकी प्लेट
- अंटार्कटिक प्लेट
- अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली अपसारी विवर्तनिकी का अच्छा उदाहरण है।
- अभिसारी विवार्त्मिकी से अन्तःसाgरीय खण्ड एवं गर्त उत्पन्न होते हैं। अभिसारी विवर्तनिकी से प्लेटों पर विनाशात्मक भूकम्पों की बाहुल्यता रहती है।
पृथ्वी की आतंरिक संरचना
भूपर्पटी
- यह पृथ्वी के आयतन का 0.5% घेरे हुए है।
- मेंटल भूपर्पटी के नीचे है और पृथ्वी के आयतन का 83% भाग घेरे हुए है।
सियाल – ऊपर की भूपर्पटी
- पृथ्वी का सबसे उपरी भाग
- रासायनिक बनावट-एल्युमिनियम
- अवसादी एवं ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है।
- महाद्वीप की रचना सियाल में मानी जाती है।
सीमा – मेंटल
- सिलिकन (Si) और मैग्नीशियम (Mg) तत्वों की प्रधानता
- इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा बाहर आता है।
- मेंटल भूपटल के मध्य असम्बद्ध सतह है, जिसकी खोज ए. मोहलोविस ने की थी। इसे मोहलोविस असंबद्धता कहते हैं।
निफे – कोर
- पृथ्वी का केन्द्रीय भाग है।
- इसकी रचना निकेल और लोहे से हुई है।
- पृथ्वी का कोर भाग ठोस है, कोर भाग पर आच्छादित परते अर्द्ध-ठोस या प्लास्टिक अवस्था में हैं।
- एस्थेनोस्फीयर विशेष परत न होकर मेंटल का ही भाग है।
- अन्तरम या क्रोड पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। इसे बेरीस्फीयर भी कहा जाता है।

चट्टान
- धरातल से 16 किमी. की गहराई तक 95% भूपर्पटी चट्टानों से निर्मित है।
- लगभग 2000 विभिन्न खनिजों में 12 खनिज ऐसे हैं, जिन्हें चत्त्तन बनाने वाले खनिज कहते हैं। इनमें सिलिकेट सबसे महत्वपूर्ण है।
- पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ चट्टान या शैल कहलाते हैं।
- आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टान व् ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं।
- आग्नेय शैलों में लोहा, मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिज अधिक होते हैं।
- आग्नेय शैलों में पाए जाने वाले खनिज हैं- चिम्ब्कीय खनिज, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, हीरा तथा प्लैटिनम।
- बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगुर कहते हैं।
- आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
- बेसोलिथ सबसे बड़े आतंरिक चट्टानी पिंड हैं। यू.एस.ए. इदाहो बेसोलिथ, प. कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिया मूलतः ग्रेनाइट के बने हैं।
- अवसादी चट्टानों में क्षैतिज रूप से जमने वाले मैग्मा को सिल कहा जाता है।
- अवसादी चट्टानी प्रदेश में लम्बवत रूप से लगने वाला मैग्मा डाइक कहा कहलाता है।
- खनिज तेल अवसादी शैलों के अंतर्गत आता है।
- वायु निर्मित शैलों में लोयस प्रमुख हैं, जबकि हिमानीकृत शैलों में मोरेन प्रमुख है।
- नाइस का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में होता है। क्वार्टजाइट का प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आग्नेय शैल
- द्रवित मैग्मा के जमने के जमने से – उदाहरण भारत का दक्कन पठार (दक्कन ट्रैप)
- ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि इसके उदाहरण हैं।
- जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
- अत्यधिक कठोर व् भारी।
अवसादी शैल
- विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से या जीव जंतुओं और पेड़- पौधों के जमाव से।
- उदाहरण- चुना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेलखड़ी, डोलोमाइट, कोयला, पीट आदि।
- जीवाश्म पाए जाते हैं।
- कठोर व भारी
कायांतरित शैल
- अत्यधिक ताप व् दबाव के कारण आग्नेय या अवसादी के रूप परिवर्तन से।
- उदाहरण- नाइस, क्वार्टजाइट, संगमरमर, प्लेट, ग्रेफाइट।
- जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
- कम कठोर व कम भारी
भ्रंशन
- दो भ्रंशों के बीच धंसी हुई भूमि को भ्रंश घाटी कहा गया है, यह लम्बी, संकरी और गहरी हुआ करती है। जर्मन भाषा में इसे गैब्रन कहते है।
- वास्जेस और ब्लैक फारेस्ट नामक पर्वतों के बीच यूरोप की प्रसिद्द भ्रंश घाटी है, जिसमे राइन नदी प्रवाहित होती है।
- एशिया स्थित जार्डन की प्रसिद्ध भ्रंशघाटी समुद्र तल से भी नीची है।
- मृत सागर नामक झील भ्रंश घाटी में स्थित है।
- संसार की सबसे लम्बी भ्रंश घाटी जार्डन घाटी से आरम्भ होकर लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका की जाम्बेजी नदी तक विस्तृत है।
- असम की ब्रह्मपुत्र घाटी रैम्प घाटी का उदाहरण है, जो हिमालय पर्वत और असम पठार के मध्य स्थित है।
- यूरोप का हार्स, ब्लैक फारेस्ट और बास्जेज भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
- डाइक – दीवार के समान खड़ी आग्नेय चट्टान।
- पृथ्वी के स्थलमंडल का लगभग ¾ भाग अवसादी शैलों से ढका है।
- पवन द्वारा दूर तक ढोए महीन बालू के कणों से निर्मित अवसादी चट्टान का अच्छा उदाहरण लोएस है, जो उत्तर-पश्चिम चीन में पाया जाता है।
- हिमानी द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है- गोलाश्म मृत्तिका।
- सेंधा नमक, जिप्सम तथा शोरा , रासायनिक विधि से बनी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं।
- धरातल के एक भाग का अपनी समीपी सतह से उठ जाने को उत्थान या उभार कहते हैं।
- भारत में कच्छ खाड़ी की लगभग 24 किमी. भूमि ऊपर उठ गयी है। यह भूमि अल्ला बांध के नाम से प्रसिद्ध है।
- धरातल के एक भाग का अपने समीपी सतह से नीचे धंस जाना निमज्जन कहलाता है।
- अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के किनारे डूबी हुई घटिया पाई जाती हैं एवं गंगा के डेल्टाई भाग में भी कोयले की तहें समुद्रतल से अधिक गहराई पर मिलती हैं।
- हिमालय आल्पस आदि पर्वतों से अधिक्षिप्त वलन प्रकार के ग्रीवा खंड मिलते हैं। ग्रीवा खंड भूपटल पर जटिल संरचना का परिचायक है।