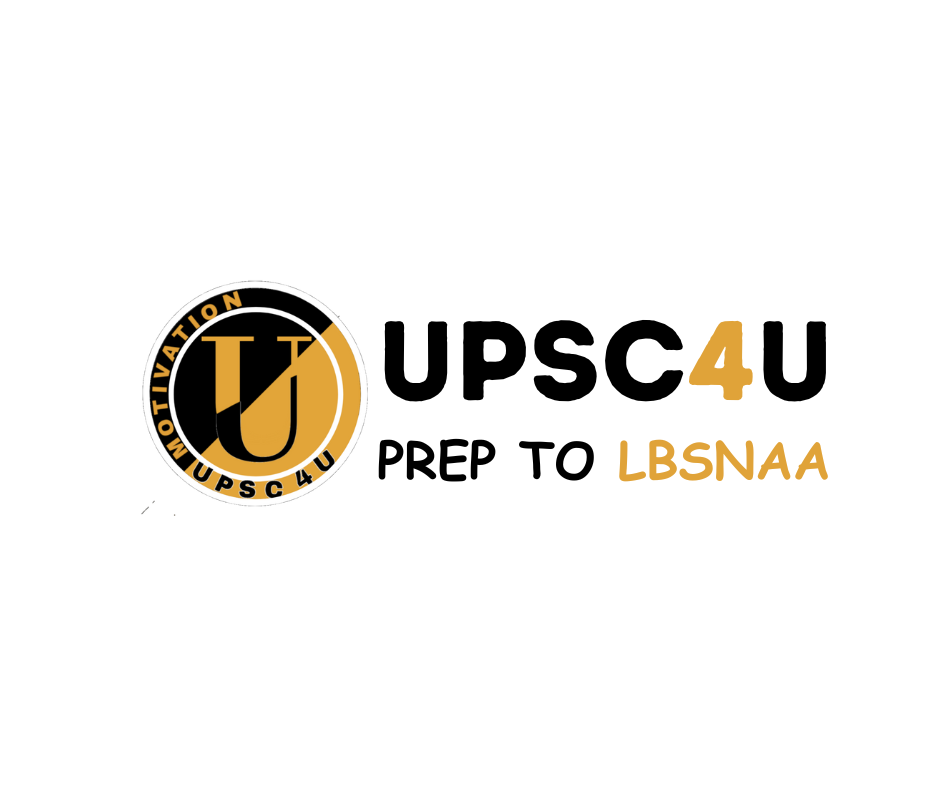कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभाग -संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 145 वीं रिपोर्ट में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में महत्त्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से निपटने के लिए की गई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE Act), 1946 के तहत कार्य करती है। हाल के वर्षों में, CBI की स्वायत्तता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं। इसे “पिंजरे का तोता” (Caged Parrot) कहकर आलोचना की गई है, जिससे इसके सुधार की मांग तेज हो गई है। यह लेख CBI में सुधार की आवश्यकता, इसके कारण, और सुझावों पर चर्चा करता है, जो UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्वपूर्ण है।
CBI में सुधार की आवश्यकता क्यों?
- राजनीतिक हस्तक्षेप:
CBI पर अक्सर सत्तारूढ़ दल के हितों को आगे बढ़ाने का आरोप लगता है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करना और सत्तापक्ष के नेताओं को संरक्षण देना इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। उदाहरण के लिए, बोफोर्स घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम जैसे मामलों में देरी और विवाद इसके प्रमाण हैं। - कानूनी सीमाएं:
DSPE Act, 1946 के तहत CBI को राज्य में जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति चाहिए (अनुच्छेद 6)। कई राज्यों (जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु) ने सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिससे इसकी जांच क्षमता सीमित हो गई है। - स्वायत्तता की कमी:
CBI कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधीन कार्य करती है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत है। यह प्रशासनिक नियंत्रण इसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण मामले (1997) में इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कदम सुझाए थे, लेकिन पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हुआ। - कर्मचारी और संसाधन की कमी:
संसदीय समिति (2023) के अनुसार, CBI में 7295 स्वीकृत पदों के मुकाबले 1709 रिक्त हैं। यह इसकी जांच क्षमता को कमजोर करता है। - पारदर्शिता का अभाव:
RTI अधिनियम के दायरे से बाहर होने के कारण CBI की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है, जिससे जनता का भरोसा कम हुआ है।
सुधार के लिए सुझाव
- कानूनी ढांचे में बदलाव:
दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति (2007) और संसदीय स्थायी समिति (2007-08) ने सुझाव दिया कि CBI के लिए एक नया कानून बनाया जाए। यह इसकी स्थिति, शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट करेगा, जिससे राज्य सहमति की बाधा दूर होगी। - स्वायत्तता सुनिश्चित करना:
CBI को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त कर एक स्वतंत्र संस्था बनाया जाए, जैसे CAG या चुनाव आयोग। विनीत नारायण मामले के निर्देशों को लागू करना जरूरी है। - नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार:
वर्तमान में CBI निदेशक की नियुक्ति एक समिति (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, और CJI) द्वारा की जाती है। इसे और पारदर्शी बनाकर बहुदलीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। - संसाधन और प्रशिक्षण:
रिक्तियों को भरने, आधुनिक तकनीक से लैस करने और नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था से CBI की दक्षता बढ़ेगी। - जवाबदेही और पारदर्शिता:
संसदीय समिति द्वारा निगरानी और चुनिंदा मामलों में जनता के लिए जानकारी उपलब्ध कराने से विश्वसनीयता बढ़ेगी।
UPSC के लिए प्रासंगिकता
- GS Paper-II (Polity & Governance): CBI की स्वायत्तता और संघवाद पर इसका प्रभाव एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न जैसे “CBI की जांच शक्ति और राज्य सहमति संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करती है?” मेन्स में पूछे जा सकते हैं।
- GS Paper-III (Internal Security): संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से निपटने में CBI की भूमिका।
- करंट अफेयर्स: हाल के घटनाक्रम, जैसे म्यांमार भूकंप जांच में सहयोग या पश्चिम बंगाल बनाम केंद्र विवाद (2024), प्रीलिम्स में संभावित हैं।
निष्कर्ष
CBI में सुधार न केवल इसकी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए जरूरी है, बल्कि यह भारत के शासन तंत्र और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भी अनिवार्य है। एक स्वतंत्र, पारदर्शी और सशक्त CBI भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। UPSC अभ्यर्थियों को इस टॉपिक को स्टैटिक और डायनामिक दोनों पहलुओं से तैयार करना चाहिए।
CBI सुधार, CBI स्वायत्तता, UPSC Polity, DSPE Act, भ्रष्टाचार जांच, संघवाद और CBI।